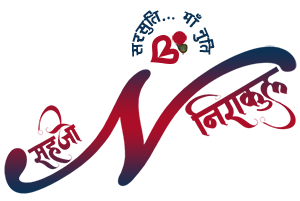
Close
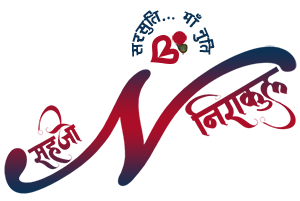
अपनी प्रशंसा स्वयं करना
एक बार भी ठीक नहीं है,
दूसरों की प्रशंसा बार-बार करना ठीक है ।
एक बात और है,
कि दूसरों के द्वारा अपनी प्रशंसा
बहुत बार हो तो भी ठीक है ।
मुझसे हाई…को
प्रशंसा पर की पारखी बनाती
स्व खुरापाती ।
यदि वर्तमान में १६ बानी,
१०० टंच स्वर्ण के समान
शत-प्रतिशत शुद्ध आत्मतत्त्व है
तो इधर-उधर की बातों में,
विषय कषायों के सेवन में,
छोटे-बड़ों के चक्कर में,
आर्त-रौद्र ध्यान में क्यों लगा है ?
इस अवस्था में रहते हुए भी
वर्तमान में अपने आपको
सिद्धों की सानी में रखना
एक प्रकार का अज्ञान है
अथवा आगम का सापेक्ष ज्ञान नहीं है ।
स्वयं को धोखा देना है ।
दूसरों को भी धोखे में डालना है ।
आचार्यों का कथन है
कि धोखा- बाजी को धोकर नष्ट करो
अन्यथा हम अवश्य धोखा खायेंगे ।
धोखा में धो और खा ये दो अक्षर हैं
जिनसे निकलता है
कि जो धोखा करेगा,
वह धोखा खायेगा ।
अतः धोखा देना छोड़ देना चाहिए ।
मुझसे हाई…को
जरूर…कल खिलाया होगा,
तभी, धोखा खाया है
आज तक मोक्षमार्ग में जो कोई भी चढ़ा है
वह नियम से नीचे गिरा है ।
जैसे-झूला झुलाने से
सर्वप्रथम ऊपर की ओर जाता है
फिर नियम से नीचे की ओर
आता ही है
बिना नीचे उतरे झूला
और अधिक ऊपर नहीं चढ़ सकता ।
नीचे गिरने के भय से
जो ऊपर चढ़ने का प्रयास नहीं करता
वह कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता ।
मुझसे हाई…को
उठ, गिर के फिर,
चीटीं जा बैठी गिरी के सिर
आज तक मोक्षमार्ग में जो कोई भी चढ़ा है
वह नियम से नीचे गिरा है ।
जैसे-झूला झुलाने से
सर्वप्रथम ऊपर की ओर जाता है
फिर नियम से नीचे की ओर
आता ही है
बिना नीचे उतरे झूला
और अधिक ऊपर नहीं चढ़ सकता ।
नीचे गिरने के भय से
जो ऊपर चढ़ने का प्रयास नहीं करता
वह कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता ।
मुझसे हाई…को
उठ, गिर के फिर,
चीटीं जा बैठी गिरी के सिर
“कर्तृत्व, भोक्तृत्व एवं स्वामित्व
बुद्धि के कारण ही दुनिया पागल हो रही है । कर्तृत्व के कारण अहंक्रिया पुष्ट होती है,
भोक्तृत्व के कारण
लोभ कषाय के साथ-साथ
अहंक्रिया पुष्ट होती है
तथा स्वामित्व के कारण
जो अपना नहीं है
उस पर भी अपना अधिकार
जमाना चाहते हैं ।”
दूसरों को किंकर बनाकर
स्वयं स्वामी बनना चाहते हैं ।
उक्त तीनों बुद्धि के कारण ही
सारा संसार अशान्ति का अनुभव कर रहा है अतः अगर शान्ति चाहते हो
तो कर्तृत्वादि बुद्धि से
विमुख होने का प्रयास करो ।
मुझसे हाई…को
हा ! कर्त्ता, भोक्ता, स्वामी बन
अधूरा मोक्ष सुपन
आचार्य श्री जी
अध्यात्म का चिन्तन,
एकत्व निश्चयगत तत्त्व के प्रति
श्रद्धान होना
यह अत्यन्त सौभाग्य की बात है ।
अध्यात्म का आश्रय लेने वाला कभी
अशान्त नहीं रहता ।
अध्यात्म के द्वारा
समस्त अशान्ति के कारणों का
निराकरण किया जा सकता है ।
अतः शान्ति की प्राप्ति के लिए
दुनिया में कहीं और नहीं जाना है
किन्तु दुनिया से वापस लौटकर
अपने आपमें आना है ।
यहीं शान्ति का खजाना है ।
दुनिया के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहो
तो बहुत जल्दी जुड़ जाता है ।
इन सम्बन्धों को यदि छोड़ना चाहो
तो गुमसुम होकर शान्त बैठ जाओ ।
कोई कुछ पूछे, तो उत्तर मत दो ।
क्या करें ! आज लगता तो ऐसा ही है
कि जैसा आचार्यों ने कहा है
वैसा ही करें ।
किन्तु कब ऐसा करें ?
बार-बार यही विचार आता है ।
परन्तु क्या करें ।
मुहूर्त ही नहीं आता है ।
ऐसा कह देते हैं ।
ध्यान रखो जोड़ने के लिए
संसार में मुहूर्त की व्यवस्था की गई है,
छोड़ने के लिए नहीं ।
जैसे-शादी/विवाह के बन्धन के लिए
मुहूर्त की व्यवस्था की गई है
किन्तु तलाक के लिए
आज तक किसी को
मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती ।
मुहूर्त देखकर संसार को
नहीं छोड़ा जाता ।
इस प्रकार बाह्य सम्बन्धों से
जितनी दूरी होती चली जायेगी
हम उतनी ही शीघ्रता से
अपने पास आते जायेंगे ।
जो शान्ति का खजाना है,
उसे प्राप्त कर लेंगे ।
मुझसे हाई…को
करते कुट्टी,
‘बेमुहूर्त’
भोगों से भी तो, लो छुट्टी
जब कोई जौहरी की दुकान पर आता है तो पहले मुनीम को बुलायेंगे,
उससे चाबी मंगवायेंगे,
फिर कमरे के अन्दर कमरे में जाकर
अलमारी के अन्दर पेटी,
पेटी के अन्दर डिब्बा,
डिब्बे के अन्दर डिब्बी,
डिब्बी के अन्दर पुड़िया,
पुड़िया के अन्दर एक और पुड़िया
उसके अन्दर एक और
गुलाबी कागज की सुन्दर पुड़िया
खोलने पर चमकता हुआ
रत्न दिखता है ।
दिखाते समय कह देते हैं,
मात्र देखो, छुओ मत,
इसके बाद रत्न खरीदने को मिल पाता है ।
रत्नों की कितनी सुरक्षा होती है ।
सुनिए यह धर्म इन हीरे, जवाहरातों से भी
अधिक महिमावन्त है, अमूल्य है,
इसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती ।
धर्म वह है जो धन को पीछे छोड़ देता है,
धन को अपनी दृष्टि से ओझल कर देता है
और आत्मतत्त्व को हमेशा
अपनी दृष्टि का विषय बनाकर चलता है ।
धर्म एक ऐसी महत्त्वपूर्ण वस्तु है
जो जीवन में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त होती है
धर्म हीरे से अधिक मूल्यवान वस्तु है
उसे अत्यधिक सम्हालकर रखने की आवश्यकता होती है ।
हीरे का नग नोट की भाँति
हाथ में रहने से मैला नहीं होता ।
मुझसे हाई…को
रतन…रत न,
हाथों में ले, नोट होते है मैले ।
स्वामित्व बुद्धि का त्याग करने के लिए ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध का प्रयोग कीजिए ।
पर पदार्थों के साथ ज्ञेय-ज्ञायक भाव रखने से स्वामित्व बुद्धि छूटना प्रारम्भ हो जाती है ।
यह विचार करो
कि जो दिख रहा है,
अथवा जिसको मैं जान रहा हूँ
वह ज्ञेय है
और जानने वाला मैं ज्ञाता हूँ ।
पर को पर के रूप में,
स्व को स्व के रूप में जानना
ज्ञेय-ज्ञायकपना है ।
जिस वस्तु का वियोग हुआ
वह वैसी की वैसी ही है ।
चार तोला थी, तो चार तोला ही है
लेकिन उसके वियोग में
व्यक्ति का १० किलो वजन कम हो जाता है । जिसको वह वस्तु मिली
उसका वजन बढ़ जाता है ।
ऐसा क्यों हुआ ।
उस सोने से ममत्व होने के कारण
मुझसे हाई…को
चीजें ज्ञेय… मैं ज्ञाता,
जाने क्यूँ ?
जड़ पे झुक जाता
लोग पूछते हैं
काम, भोग, बन्धकथा से
मुक्ति कैसे संभव है ?
काम-भोग-बन्ध की सामग्री से परिपूर्ण इसी संसार में भगवान् भी रहते हैं ।
शब्द ज्ञान उनको भी है
भले ही कान से नहीं सुनते ।
बल्कि अतीन्द्रिय स्वरूप केवलज्ञान से
वे सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं,
उनसे कुछ भी अनजाना
और अनदेखा नहीं है
फिर भी वे काम-भोग- बन्ध कथा से
पूर्णतः पृथक् हैं,
इनसे उनका कभी कोई मिलन नहीं होता,
उन्हें इनका अनुभव भी नहीं होता
क्योंकि भगवान् तो हमेशा
एकत्व विभक्त आत्मस्वरूप का
अनुभव करते हैं ।
आश्चर्य तो होता है कि,
ऐसा कैसे सम्भव है ।
फिर भी आचार्यों ने युक्ति देकर
समाधान दिया है ।
संसार में अनन्त पदार्थ हैं ।
उनके प्रति ग्राह्य-ग्राहक भाव
बन्धकथा को उत्पन्न करता है ।
जबकि ज्ञेय-ज्ञायक भाव
उनसे मुक्ति दिलाता है ।
भगवान् का अनन्त पदार्थों के साथ
मात्र ज्ञेय ज्ञायक भाव होता है
फलस्वरूप वे बन्ध के साथ
एकत्व को प्राप्त नहीं होते
अतः उसका अनुभव भी नहीं करते,
किन्तु काम-भोग-बन्ध से मुक्त रहते हैं ।
संसारी प्राणी स्वयं पर पदार्थों से कर्तृत्व, भोक्तृत्व एवं स्वामित्व भाव रखता है
इसलिए बन्ध को प्राप्त होता है ।
संसार के पदार्थ हमसे चिपकते हैं
या हम पदार्थों से चिपकते हैं ।
यदि पदार्थ आकर जीव से चिपकते हैं
तो भगवान् से भी चिपकना चाहिए
जबकि समवसरण में भगवान् के चरणों में सारा दिव्य वैभव लोटता है
फिर भी भगवान् उसकी ओर
आँख उठाकर भी नहीं देखते हैं ।
यहाँ तक कि वे
सिंहासन से चार अंगुल ऊपर ही
आसीन रहते हैं ।
इससे स्पष्ट है
कि पदार्थ हमसे नहीं चिपकते
किन्तु हम अपने ममत्व भाव के
कारण पदार्थ से चिपकते हैं ।
मुझसे हाई…को
श्री जी ने छुई ना,
मुँह मोड़ो…किसी की श्री हुई ना
एकेन्द्रिय जीव के सबकी अपेक्षा
बन्ध कम होगा ।
द्वीन्द्रियादि जीवों में एक-एक इन्द्रिय का विकास होता चला जाता है ।
तत्सम्बन्धी उसका ज्ञान भी
विकसित होता जाता है ।
जितना-जितना ज्ञान बढ़ेगा
उतना-उतना काम, भोग कथा का परिचय
एवं अनुभव बढ़ता जाता है ।
फलतः बन्ध भी अधिक होता है ।
संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव के
सबसे अधिक बन्ध होता है ।
उसी पञ्चेन्द्रिय जीव के काम भोग से
जितना परिचय कम होगा
उतना बन्ध भी कम होगा ।
संक्लेश या आसक्ति का भाव
अधिक होने से बन्ध भी अधिक होता है
और विशुद्धि एवं अनासक्ति का भाव
अधिक होने से बन्ध कम होता है ।
जितना परिचय होगा
उतना ही संक्लेश होगा,
जितना कम परिचय होगा
उतनी विशुद्धि बढ़ेगी ।
संयोग के द्वारा संसारी प्राणी पर
दुःख का पर्वत टूट पड़ता है
क्योंकि संयोग में आदमी रच-पच जाता है
परन्तु जब उनका वियोग होता है
तो अकेला रह जाता है
अतः दुःखी होता है ।
सोचो तो ! सिद्ध परमेष्ठी
अनन्त काल तक अकेले कैसे रहते होंगे ।
मुझसे हाई…को
पर…चय में लागा ,
नाभि कस्तूरी मृग अभागा
काम, भोग, बन्धकथा एवं
एकत्व विभक्त आत्मकथा के अतिरिक्त
आगम में चार प्रकार की कथाओं का
वर्णन किया है
१. संवेगनी, २. निर्वेगनी, ३. आक्षेपणी
और ४. विक्षेपणी ।
इनमें से प्रारम्भ की दो कथायें वैराग्यपरक है । इनके श्रवण से संसार से भय भी होता है ।
पापों से भीति भी होती है
एवं संसार, शरीर, भोगों से
वैराग्य उत्पन्न होता है ।
वैराग्य दृढ़ भी होता है ।
आक्षेपणी और विक्षेपणी कथायें
बुद्धि को सन्तुलित
एवं बुद्धि को पैनी करने के लिए
प्रयुक्त होती हैं ।
सभी के लिए इन दो कथाओं के
प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया गया । समाधि के समय
अन्तिम दो कथाओं का श्रवण
नहीं कराया जाता ।
समाधि के समय तो
संवेगनी, निर्वेगनी कथाओं का श्रवण
एवं उन्हीं से सम्बन्धित धर्मोपदेश
श्रवण कराने को कहा गया है ।
सामान्य धर्मोपदेश के समय भी
इन्हीं कथाओं का उपदेश दिया जाता है । धर्मोपदेश का अर्थ
भी यही किया है
कि ६३ शलाका पुरुषों के
जीवन-चरित्र का कथन करना ।
जिससे पापों से भीति हो जाए
और पुण्यार्जन का भाव जागृत हो जाये,
ऐसा ही उपदेश धर्मोपदेश माना गया है ।
इन कथाओं के उपदेश श्रवण से
पाप-पुण्य का फल
एवं जीवन में उतार चढ़ाव के कारण
विदित होते हैं ।
मुझसे हाई…को
कम ना,
क ? … था
हमारा इति…हास, लगता पता
आचार्य श्री जी
ज्ञान को दर्शन के समान
बनाने का प्रयास करना
आध्यात्मिक साधक की सर्वोत्कृष्ट साधना है ।
ज्ञान के साथ ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध बनता है । ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध अपने आप में
बहुत महत्त्वपूर्ण है ।
इसमें स्व और पर सभी को
ज्ञेय बनाने की प्रक्रिया चलती है ।
दर्शन में ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध नहीं होता । अनुमान, व्याप्ति, तर्क, स्मृति,
प्रत्यभिज्ञान, अवग्रह, ईहा, अवाय,
धारणा आदि भी ज्ञानोपयोग की यात्रा में हैं ।
यदि ज्ञान को दर्शन जैसा
निर्विकल्प बनाना है
तो ज्ञान की यात्रा को पीछे
रिवर्स में लौटाना होगा ।
स्मृति, तर्क, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान, धारणा, अवाय, ईहा अवग्रह तक रिवर्स में आना पड़ेगा । ज्ञान की यात्रा अवग्रह तक आते-आते निर्विकल्प दर्शन जैसी हो सकती है ।
हालाँकि ज्ञान दर्शन रूप नहीं हो सकता
और दर्शन ज्ञान रूप नहीं हो सकता
क्योंकि ये दोनों पृथक् पृथक् गुण हैं ।
एक गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं होता,
यह वस्तु-व्यवस्था है ।
फिर भी ज्ञान को विकल्पजाल से
हटाने के लिए
ज्ञान को दर्शनवत् बनाओ, ऐसा कहा ।
ज्ञान का जो विषय है
वह ज्ञान ही बनायेगा
और दर्शन के योग्य विषय को
दर्शन ही विषय बनायेगा ।
ज्ञान का विषय दर्शन
और दर्शन का विषय ज्ञान बनाये
ऐसा कभी नहीं होता ।
छद्मस्थ अवस्था में ये दोनों
एक साथ नहीं होते,
इनके विषय भी कभी परिवर्तित नहीं होते । दर्शन वस्तु के सामान्य अंश को
विषय बनाता है
और ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है ।
ज्ञान वस्तु के आभास मात्र को ग्रहण करके निर्विकल्प रह सकता है
अर्थात् ‘वस्तु है’ मात्र इतना जानना ।
क्या है ? किसकी है ? कहाँ है ?
क्यों है ? आदि विकल्प न करे ।
यही ज्ञान की निर्विकल्प यात्रा है ।
इस निर्विकल्प यात्रा में अच्छा-बुरा, राग-द्वेष, आदि अवकाश नहीं पा सकते ।
इस प्रकार का रागादि रहित
निर्विकल्प ज्ञान ही
केवलज्ञान की प्राप्ति में कारण होता है ।
मुझसे हाई…को
ज्ञान दर्पण सा,
दर्शन सा कर लो
…सँवर को
आचार्य श्री जी
यदि कोई कहता है कि
आप ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लो
मुझे नहीं करना ।
मुझे इतना धर्म नहीं करना ।
अब क्या करें ?
उसका उपादान ही जागृत नहीं है
तो क्या करें ?
किसी का उपादान जागृत हो
तो फिक्र की जा सकती है ।
आज सबको दूसरे की चिन्ता है
कि उसका क्या होगा ?
आचार्य कहते हैं,
किसका क्या होगा ?
सब कुछ छोड़ दिया
अब किसकी चिन्ता करता है ?
संसार में यही सबसे बड़ा व्यवधान है
कि उसका क्या होगा ?
साधक बनने के उपरान्त भी
पूर्व सम्बन्धी जनों की चिन्ता रहती है ।
व्यवहार की अपेक्षा से
ये उनके पूर्व के माँ-पिता थे
इत्यादि स्वीकार करना ठीक हैं,
लेकिन यह ध्यान रखो
कि व्यवहार एक ऐसा जाल है
जो बहुत दूर जाने के उपरान्त भी
नहीं छूटता है ।
कुछ ऐसे भी व्यवहार होते हैं
जो सच्चे होते हैं
लेकिन सच्चे होकर भी
निश्चय के सामने
वे सभी फीके नहीं हो पा रहे हैं ।
निश्चय का रस आना चाहिए ।
शुद्ध-बुद्ध चेतना का रस आना चाहिए ।
चेतना का रस आते ही
वे सभी फीके हो जाते हैं ।
सभी बाह्य सम्बन्ध छूट जाते हैं ।
मोक्षमार्ग अकेले का है ।
निश्चय मोक्ष मार्ग
और भी अधिक अकेले का है ।
व्यवहार का निभाना
अत्यन्त कठिन होता है ।
निश्चय बहुत सरल है
क्योंकि इसमें परिश्रम नहीं होता,
थकान नहीं होती,
विकल्प नहीं होते ।
मुझसे हाई…को
भींगे कितने रस चिच्चेतना,
से पूछो आत्मा से
आचार्य श्री जी
धवला आदि ग्रन्थों में
दिट्ठमग्गो शब्द आया है ।
इसका अर्थ है
कि जिसने मार्ग को देख लिया है ।
एक बार वस्तु को देख लेने के बाद
टॉर्च की आवश्यकता नहीं होती ।
इसी प्रकार जिसने मार्ग को देख लिया
उसे मार्ग की शाब्दिक परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती ।
जैसे-जो सीढ़ी चढ़ने का अभ्यस्त है,
वह इधर-उधर बात करते हुए
सीढ़ी को देखे बिना भी चढ़ता जाता है ।
गुलाटी खाकर गिरता नहीं है,
किन्तु बिना अभ्यास के
प्रारम्भ में एक-एक सीढ़ी को देखकर,
आजू-बाजू में लगे हुए
पाइप की रेलिंग को पकड़कर चलते हैं
जिससे चूक न जाए ।
यदि चूक भी जाए
तो धड़ाम से नीचे न गिर जाए
इसलिए पाइप का सहारा लेना
आवश्यक होता है ।
इसी प्रकार जो दिट्ठमग्ग होते हैं
वे यदि मार्ग से
या सम्यग्दर्शन से
नीचे मिथ्यात्व में आ जाते हैं
तो अन्तर्मुहूर्त में बिना करण किए
शीघ्र ही पूर्व विशुद्धि के बल पर
सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेते हैं ।
यह दिट्ठमग्ग का प्रभाव है ।
बार-बार आत्मा की आराधना
करने वाला व्यक्ति
शेष द्रव्यों से प्रभावित नहीं होता है ।
यदि कर्मोदय में मन कहीं चला भी जाए
तो अभ्यास होने के कारण
उसे शीघ्र ही अपने
आत्मतत्त्व की ओर वापस लौटा लेता है
मुझसे हाई…को
देखा मार्ग
दें खो मार्ग
…झूठ
दिद्ठ-मग्ग अनूठ
आचार्य श्री जी
एक मत में ‘नेति’ को स्वीकार किया है ।
इसका अर्थ बहुत गंभीर है ।
इसे समीचीन दृष्टिकोण से देखें
तो इसका इस प्रकार
प्रयोग किया जा सकता है ।
‘नेति’ का अर्थ क्या है ?
‘इस प्रकार नहीं है’
अथवा ‘यह नहीं है’ ।
व्यवहार नय कहता है
न इति,
तो निश्चयनय भी कहता है
न इति
यह आत्मा नहीं है,
आत्मा ऐसा नहीं है ।
व्यवहारनय की दृष्टि में
निश्चयनय का विषय
न इति रूप है
और निश्चयनय की दृष्टि में
व्यवहारनय का विषय
नेति रूप होता है ।
जैसे-एक पेन है
उसका कथन नेति मान्यता में कैसे होगा ?
यह पेंसिल नहीं है,
यह पुस्तक नहीं है,
यह बेंच नहीं है, इत्यादि
तो क्या है ?
इस प्रश्न के उत्तर में यह पेन है,
ऐसा कथन नहीं करेंगे ।
जैसे-आत्मा है
उसका कथन नेति मान्यता में
इस प्रकार होगा
कि-यह पुद्गल नहीं है,
यह धर्मद्रव्य नहीं है,
अधर्मद्रव्य नहीं है,
आकाशद्रव्य नहीं है,
कालद्रव्य नहीं है ।
फिर क्या है ?
ये सब नहीं है, बस जो है सो है ।
आत्मा स्पर्शवान नहीं है,
रसवान नहीं है,
गन्धयुक्त नहीं है,
वर्णवान नहीं है,
शब्द से रहित है ।
फिर आत्मा क्या है ? कैसा है ?
तो ये सब नहीं है, बस जो है सो है ।
नेति मान्यता एकान्त स्वरूप है
तो मिथ्या है
यदि वही अस्ति-नास्ति रूप
अनेकान्त स्वरूप है तो सम्यक् है ।
आत्मा के इस स्वरूप के प्रति
क्यों नहीं है हमारा उपयोग ?
आत्मस्वरूप में क्यों नहीं ठहरता ?
रास्ता नहीं मिलता क्या ?
अरे, ठहरने के लिए
रास्ते की आवश्यकता नहीं होती ।
ठहरने की बात की जा रही है,
चलने की नहीं ।
चलना हो तो मार्ग की जरूरत पड़ती है ।
ठहरने से मंजिल कैसे मिलेगी ?
मिल जायेगी ।
आज तक आत्मस्वरूप में
नहीं ठहरने के कारण ही
मुक्ति मंजिल की प्राप्ति नहीं हुई ।
स्वरूप में रुकना नहीं हो पा रहा है
जबकि घूमकर के यहीं आना पड़ेगा ।
स्वरूप में यात्रा को विश्राम देना पड़ेगा
तभी संसार-परिभ्रमण से मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं ।
मुझसे हाई…को
क्या फलां फलां चीज मैं ?
नेति-नेति
चिच्-चिदेव मैं
आचार्य श्री जी
वीतरागी
रागी में भी वीतरागता का दर्शन करता है
लेकिन रागी
वीतरागी में भी राग का अनुभव करता है ।
जैसा चश्मा होगा,
जैसी दृष्टि होगी
वैसा ही पदार्थ देखने में आता है ।
निश्चय का चश्मा लगाने के उपरान्त
राग की पर्याय नहीं दिखती
किन्तु मूल पदार्थ दिखता है ।
हीरे का नग भले ही कीचड़ में फँसा हो
लेकिन हीरे का नग तो हीरा ही माना जाता है । जौहरी उस समय कीचड़ से परहेज नहीं करता वरन् उसे उठाकर
हाथ एवं नग को स्वच्छ करके
हीरे का दर्शन कर लेता है ।
जौहरी की दृष्टि में
एक मात्र हीरा दिखता है
चूँकि हीरे की ओर ही
उसका उपयोग रहता है ।
इसी तरह वीतराग दृष्टि वाले को
सर्वत्र वीतरागता का दर्शन होता है ।
वह एकत्व निश्चय को प्राप्त
सिद्धत्व का अवलोकन करता रहता है
इसलिए हर्ष विषाद नहीं करता ।
हर्ष-विषाद करने से
एकत्व की क्षति होती है ।
निश्चय दृष्टि लुप्त हो जाती है ।
वीतरागता भी समाप्त हो जाती है ।
हर्ष विषाद नहीं करने से
यथावत् शान्ति प्राप्त होती है ।
भेदविज्ञान का प्रयोग किए बिना
श्रद्धा का विषय अनुभव में नहीं आ सकता । पर्यायदृष्टि से पर्याय का अवलोकन बुरा नहीं लेकिन पर्याय में मूढ़ता होना बुरा है
अतः पर्यायदृष्टि मिथ्या नहीं
किन्तु पर्याय मूढ़दृष्टि मिथ्या है ।
द्रव्य का अवलोकन भी अच्छा बुरा नहीं
किन्तु हर्ष विषाद के साथ
अवलोकन करना ठीक नहीं ।
कई लोगों का कहना है
कि पर्याय के बारे में क्या चिन्तन करना ?
द्रव्य का चिन्तन करो ।
पर्याय दृष्टि सो मिथ्यादृष्टि
ऐसा कहने वालों को
स्वयं सम्यक् रूप से विचार करना चाहिए
कि पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं है
और द्रव्य पर्याय से भिन्न नहीं है
अतः द्रव्य के साथ पर्याय का
और पर्याय के साथ द्रव्य का चिन्तन
मिथ्या नहीं हो सकता ।
पर्याय का चिन्तन करिए
परन्तु आप पर्याय में मुग्ध मत होइये ।
मैं तो सोचता रह जाता हूँ
आपकी दृष्टि की बलिहारी को देखकर
कि द्रव्यदृष्टि रखते हुए भी
आप द्रव्य संग्रह में लगे हो ।
यदि पूछा जाए कि
आप क्या पढ़ रहे हो ?
तो आप कहते हैं द्रव्यसंग्रह ।
कितना संग्रह हो गया ?
हो ही रहा है ऐसा जबाब मिलता है ।
मुझसे हाई…को
जोहरी, हटा कीचड़,
हीरा उठा ले…और चाले
आचार्य श्री जी
आचार्य कुन्दकुन्द महाराज की
कथन शैली अध्यात्ममय है ।
वे शब्दों में कभी उलझते नहीं ।
जबकि आज हम शब्दों में
उलझते चले जाते हैं ।
आचार्य देव गम्भीर से गम्भीर विषयों को
बिना किसी शब्द उलझन के
सीधी सरल शैली में
प्रस्तुत करते चले जाते हैं
उनके एक एक शब्द की गहराई में
जाने पर ऐसा लगता है
कि मौन हो जाओ,
कोई भी वाचनिक
और शारीरिक चेष्टा मत करो ।
बार-बार समयसार का
वाचन करने के उपरान्त भी
पाचन की ओर दृष्टि नहीं जाती ।
गाय, भैंस आदि पशु दिन में
घास खाकर आते हैं
और रात्रि में चर्बण करते हैं
अर्थात् जुगाली करते हैं ।
बिना जुगाली के पशु बीमार हो जाता है ।
ये रोधन्ति ते पशवः
जो रोधन (जुगाली) करते हैं,
वे पशु कहलाते हैं ।
भगवती आराधना में
आचार्य महाराज ने कहा है
कि स्वाध्याय करने वाले
दिन में स्वाध्याय करने के उपरान्त
रात्रि में ‘गइया’ गाय के समान जुगाली करें अर्थात् रात्रि में अनुप्रेक्षा, आम्नाय, चिन्तन
आदि के माध्यम से तत्त्व ज्ञान को पचा लें ।
कुछ शेष रह जाये
तो अगले दिन पृच्छना करके
पूर्ण ज्ञान (पूर्ण पाचन) कर लें ।
फिर दूसरा नया विषय ग्रहण करें ।
आज स्वाध्याय और वाचना के लिए जितना समय दिया जाता है
उससे आधा भी समय
चिन्तन के लिए नहीं दिया जाता ।
प्रत्येक व्यक्ति के पास
चिन्तन-शक्ति रहती है ।
वह उस शक्ति का कहीं न कहीं
उपयोग तो करता ही है ।
कई लोगों के पास
तो ऐसी क्षमतायें होती हैं
कि यदि वह तत्त्व-चिन्तन की
गहराई में उतर जाए
तो उसे अनेक प्रकार के
ज्ञान रूपी मोतियों की उपलब्धि हो जाती है । विपरीत चिन्तन न करें
तो चिन्तन शक्ति का उपयोग
सम्यक् चिन्तन में होगा ।
चिन्तन अपने ज्ञान की
अनुभूत्यात्मक होता है ।
चिन्तन में जो रस आता है
उसी से तत्त्वज्ञान पचता है
और वही अपने पास बचता है
उसी प्रकार स्वाध्याय रूपी भोजन का
चिन्तन रूपी जुगाली की क्रिया होती है
तब तत्त्व ज्ञान की अनुभूति,
तत्त्वज्ञान का आनन्द रूपी रस निर्मित होता है । यही ज्ञान के पाचन की क्रिया है ।
तत्त्वज्ञान बलीभूत होता है, पुष्ट होता है ।
भविष्य के लिए भी
ज्ञान संस्कार मजबूत होता है ।
अध्ययन के समय शब्द से अर्थ की
ओर गति होना चाहिए ।
अर्थ से ज्ञान और
ज्ञान से भाव प्रत्यय की ओर गति होती है
तभी स्वाध्याय की
एवं अध्यात्म रस की अनुभूति होती है ।
चिन्तन की चक्की में ही
शब्दों के अर्थ उद्घाटित होते हैं
उसके बिना नहीं ।
यदि शब्द चिन्तन में नहीं आये
बल्कि चित्त में ही रह गये
तो जैसे चक्की की कील के इर्द-गिर्द
गेहूँ पिसते नहीं हैं, ज्यों के त्यों रह जाते हैं
उसी प्रकार शब्द चित्त में रह जाते हैं
तो वे अर्थवान् न होकर
अनुभूत नहीं हो पाते ।
शब्द का अर्थ क्या है ?
यदि इस ओर दृष्टि नहीं जाती
तो स्वाध्याय का रस नहीं आता ।
अतः स्वाध्याय नहीं करो,
ऐसा नहीं कहा जा रहा है
किन्तु स्वाध्याय के साथ-साथ
अर्थ की ओर चिन्तन, मनन, अनुप्रेक्षा की
ओर भी बार-बार दृष्टि जाना चाहिए
तभी सही स्वाध्याय होगा ।
स्वाध्याय का प्रयोजन भी सिद्ध होगा । अनुप्रेक्षा करना ही ज्ञान की रोधन-क्रिया है । अनुप्रेक्षा का अर्थ ही है
कि आज जो पढ़ा है,
जो श्रवण किया उसके बारे में
बार-बार चिन्तन करना ।
द्वादश अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से ही
तत्त्व चिन्तन विकसित होता है।
‘मुहुर्मुहुश्चिन्तनं इति अनुप्रेक्षा’
चिन्तन और अनुचिन्तन में
उपयोग से ज्ञान से
अपनत्व जुड़ जाता है
और उसका चर्बण होने के कारण
रस आना प्रारम्भ हो जाता है।
मुझसे हाई…को
जा चिन्तन की चक्की में,
टूटे फूटे…शब्द अनूठे
आचार्य श्री जी
आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने
अपनी लघुता को
तथा प्राचीन आचार्यों से
उन्हें जो उपलब्ध हुआ उसकी गरिमा को
ज्यों का त्यों बनाए रखने का प्रयास किया है ।
जो जितना लघु होता है,
वह उतना महान् होता है ।
आचार्य स्वयं कह रहे हैं
कि यदि में भूल जाऊँ
तो मेरी भूल को छल के रूप में
ग्रहण मत कर लेना, यह उनकी महानता है ।
प्रायः संसारी प्राणी
अपना बड़प्पन दिखाने के लिए
जो उनसे बड़े हैं,
गौरव के स्थान हैं
उनको भी भूल कर,
यह सब मेरा ही प्रताप है,
यह सब मेरे ही पुरुषार्थ का परिणाम है
इस तरह कहता है
लेकिन आचार्य कुन्दकुन्ददेव की
लघुता को देखिए ।
जिन्होंने यह लिखा
कि वह एकत्व अपने आपमें सुन्दर है, अविसंवादनीय है,
स्वीकार करने योग्य है
हम उसको शब्दों के माध्यम से कहना चाहते हैं उसमें भूल सम्भव है
अतः छल ग्रहण नहीं करना
अर्थात् विपरीत परिणति के साथ
स्वीकार नहीं करना ।
उन्होंने कहा
कि मैं अपने बुद्धि-वैभव के द्वारा दिखाता हूँ । हालांकि उनका वह बुद्धि वैभव
सामान्य नहीं है ।
जिस बुद्धि ने रत्नत्रय को स्वीकार किया है
वह विशिष्ट बुद्धि का ही परिचय देती है ।
फिर भी उन्होंने
अत्यन्त लघुता का परिचय दिया ।
मुझसे हाई…को
बनो ल…घु
घु…ल मिल जाने,
डूबे पत्थर दिल
आचार्य श्री जी
सच श्रुतदेवता की आराधना करने बैठ जाते हैं
तो बाहर क्या हो रहा है
कुछ पता ही नहीं चलता ।
गाथाओं के चिन्तन के समय
शब्दों के अर्थों की ओर
जब ध्यान एकाग्र होता है
तब उपयोग में
साक्षात् निर्विकल्प समाधि जैसा
आनन्द आता है ।
जब चिन्तन में इतना आनन्द आता है
तो वास्तव में जब निर्विकल्प समाधि स्वरूप उपयोग होता होगा
तब कितना आनन्द आता होगा ।
चिन्तन में एकाग्रता के समय
शरीर भी अड़ोसी पड़ोसी जैसा हो जाता है । किसी साधक में यदि
शारीरिक अनुकूलता नहीं है
अर्थात् ढाई घण्टे की सामायिक
या ध्यान आदि नहीं कर सकते,
डॉक्टर ने ज्यादा देर बैठने का निषेध किया है । तो ऐसे समय श्रद्धान आस्था
अथवा धारणा के माध्यम से आत्मरुचि,
आत्मसाधना को जागृत करना चाहिए ।
ऐसी धारणा बनाना चाहिए
कि आत्मा के पास अनन्त गुणों का वैभव है । धारणा के बल पर
धीरे-धीरे वैभव से परिचय
बढ़ता चला जाता है ।
आत्मरुचि बढ़ती चली जाती है
फलतः रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग
प्रशस्त होता जाता है ।
साधक आनन्द पूर्वक मोक्षपथ पर
आह-वाह के बिना अथक-अरुक
अबाधगति से बढ़ता चला जाता है ।
साधक को हमेशा आत्मानुभव नहीं होता, हमेशा निर्विकल्प समाधि नहीं रहती ।
इसलिए निश्चय श्रुतकेवलित्व से
या भावश्रुतज्ञान से बाहर आना पड़ता है ।
बाहर आये बिना उसमें हमेशा नहीं रह सकता । साधना के क्षेत्र में ऊपर उठने के लिए
अनेक आयाम किये जाते हैं ।
तब कहीं साधक साधना की ऊँचाईयों का
स्पर्श कर पाता है ।
जैसे-आपको पर्वत के शिखर पर चढ़ना है,
तो वहाँ सीधे ही नहीं पहुँच जाते हैं
किन्तु वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता भी
घुमावदार होता है ।
दूरी ज्यादा हो सकती है ।
लेकिन चक्कर आने से बच जाते हैं ।
चक्कर को बचाने के लिए
पर्वत का चक्कर लगाना पड़ता है ।
ऊपर पहुँचने पर नीचे नहीं देखना,
क्योंकि ऊपर से नीचे देखने पर
चक्कर आते हैं ।
अतः यहाँ ऊँचाई पर कैसे चढ़ेंगे ?
इसके समाधान में आचार्य कहते हैं
कि श्रुत के माध्यम से
बाह्य द्रव्यों को सम्यक् प्रकार से जानो
लेकिन इधर-उधर बाह्य पदार्थों में अपना उपयोग मत उलझाओ ।
जो द्रव्यश्रुत केवली होते हैं
वे अपने श्रुतज्ञान से
ए टू जेड समस्त पदार्थों को जानते हैं ।
पर पदार्थों को जानने से
उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि भैय्या
इन सबमें साथ नहीं है ।
पर पदार्थों को जानते हुए
कितना भी काल व्यतीत करो,
उससे केवल नहीं होगा ।
गणधर परमेष्ठी को भी
केवलज्ञान नहीं हुआ ।
भगवान् महावीर के मुक्त हो जाने पर
दिशाबोध प्राप्त हो गया ।
ज्यों ही प्रातः भगवान् महावीर स्वामी को
निर्वाण प्राप्त हुआ,
अपनी ओर दृष्टि गई
तो शाम को गणधर परमेष्ठी को
केवलज्ञान प्राप्त हो गया ।
यही सबकी दशा है भैय्या,
अपनी ओर दृष्टि नहीं जाने से
आज तक केवलज्ञान प्राप्त नहीं हुआ ।
मुझसे हाई…को
झुक के,
थोड़ा सा घूम के,
ऊंट…
जा पर्वत के कूट
आचार्य श्री जी
पूछा जा रहा है
कि आत्मा के गुणों में हमेशा
ज्ञान गुण की ही विशेष चर्चा क्यों होती है ?
सुनिए,
कुण्डलपुर की बात है,
लगभग बीस वर्ष पूर्व की बात है ।
सम्मेलन हो रहा था,
बाहर से बहुत से विद्वान् आए थे ।
मुझसे प्रवचन का निवेदन किया ।
उस समय अपने स्वाध्याय का समय था,
अतः आचार्य अकलंकदेव का
स्मरण करके स्वाध्याय प्रारम्भ कर दिया । आचार्य अकलंकदेव ने
अनेकान्त और स्याद्वाद को
प्रस्तुत करते हुए
एक विषय प्रस्तुत किया है
कि आत्मा अचेतन है ।
सहज ही प्रश्न उठता है
कि यह कैसे सम्भव है ?
छह द्रव्यों में आत्मा ही तो चेतन है ।
‘जीवमजीवं दव्वं’
दो प्रकार के द्रव्य हैं-
जीव और अजीव ।
छह द्रव्यों में से जीव को छोड़कर
शेष पाँच द्रव्य अजीव हैं ।
ऐसा तो कहा है
परन्तु आप इन्हें अचेतन कह रहे हैं,
यह भी अजीव हो गया ।
अजीव और अचेतन में अन्तर है ।
यह कैसे ?
यह तो बिल्कुल नई बात है ।
आप लोग सिद्धचक्र विधान करते हैं,
उसमें सिद्धपरमेष्ठी को अचेतन रूप में आराधित किया है ।
यह भी कैसे ?
हम चेतन और वे अचेतन यह कैसे ?
सभी श्रोतागण एवं विद्वज्जन
आश्चर्य कर रहे हैं ।
फिर भी अनेकान्त के माध्यम से
सब सिद्ध होता है ।
सभी ने कहा-ऐसा कैसा अनेकान्त
जो जीव को अजीव या अचेतन बना दिया । सुनो, सुनो…
गुणों की अपेक्षा से
द्रव्य का विधान होता है
अर्थात् गुणों से ही द्रव्य की पहचान होती है । यदि गुण नहीं हैं
तो हम यह नहीं कह सकते
कि यह कौन सा द्रव्य है
या वह कौन सा द्रव्य है ।
द्रव्य का परिणमन पर्याय कहलाती है ।
जैसा कि तत्त्वार्थसूत्र के पंचम अध्याय में
एक सूत्र में आचार्य उमास्वामी महाराज ने
इस विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है-
तद्भावः परिणामः
अर्थात् द्रव्य का भाव होना,
प्रति समय बदलते रहना परिणाम है ।
इसी को पर्याय कहते हैं ।
द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों की समष्टि होती है । आत्मा अनन्त गुणों का पिण्ड है ।
उनमें चेतन गुण को
प्रधानमन्त्री के रूप में रख दी ।
इस गुण में जानने देखने की क्षमता होती है । चेतन के अतिरिक्त
अन्य गुणों में जानने, देखने की क्षमता नहीं है । उन समस्त गुणों की विवक्षा में
आत्मा को अचेतन कहा है ।
चेतन गुण ज्ञान, दर्शन के भेद से
दो प्रकार का है ।
जिसे ज्ञानचेतना और दर्शनचेतना
अथवा ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग के
नाम से जाना जाता है ।
इस प्रकार चेतना शक्ति के
माहात्म्य से ही जीव को चेतन कहा गया है । ज्ञानदर्शन गुण को थोड़ा-सा गौण करके
देखेंगे तो आत्मा भी
अन्य द्रव्यों की भाँति
जानने देखने का कार्य नहीं कर पायेगा,
फिर किसके बल पर उसे चेतन द्रव्य कहेंगे ।
ज्ञान गुण एक ऊधमी लड़के के समान हैं,
यह ऊधम मचाता है ।
दूसरा लड़का शान्त है,
ऊधम नहीं मचाता ।
लेकिन जो ऊधमी है,
वही कमाऊ है,
इसलिए घर में
उसकी आरती उतारी जाती है ।
इसी प्रकार ज्ञान गुण जानने की क्रिया में
सक्रिय है ।
वही समस्त द्रव्यों की पहचान कराता है ।
ज्ञान गुण के बिना
‘मैं आत्मा हूँ’ यह भी नहीं जान सकेंगे ।
ज्ञान गुण प्रकाशमय है
इसके बिना तो अन्धकार ही अन्धकार है ।
दूसरी बात की ओर भी दृष्टि करें
कि रत्नत्रय में भी ज्ञान गुण शामिल है ।
शेष सम्यग्दर्शन और चारित्र भी अचेतन हैं, क्योंकि सम्यग्दर्शन को चेतना रूप
दर्शनोपयोग में गर्भित नहीं किया गया ।
श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यग्दर्शन है ।
आचार्यों की इस विवक्षा पर
विचार करें तो यह अचेतन सिद्ध होता है ।
इस श्रद्धागुण की समीचीनता से
ज्ञान गुण में समीचीनता आती है ।
सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्याज्ञान
और चारित्र मिथ्याचारित्र कहलाता है । मोक्षमार्गी कहलाने की पात्रता का प्रादुर्भाव
इसी सम्यग्दर्शन के द्वारा होता है ।
इस प्रकार श्रद्धा गुण भी अपने आप में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है ।
मुझसे हाई…को
ज्ञान गुण भी ऊधमी थोड़ा
जैसे कमाऊ छोरा
आचार्य श्री जी
दुकानदार जितने समय तक
दुकान खोलना चाहे
उतने समय तक खोल लेते हैं
इसके उपरान्त बन्द करने का समय होता है,
तो बन्द कर देते हैं ।
दुकान बन्द तो कर देते हैं
लेकिन दुकानदार
दुकान से बाहर नहीं निकलता ।
जब तक दुकान खुली रहती है
तब तक ग्राहक आते हैं ।
उनके साथ लेन- देन की प्रवृत्ति चलती है ।
जितने ज्यादा ग्राहक आते हैं,
उतनी अधिक सन्तुष्टि होती है ।
दुकानदार कहता है-
धन्य दिवस, धन्य घड़ी, धन्य भाग्य मेरो भयो । दुकान बन्द होने पर
वह मुनीम जी से कहता है
कि मुनीम जी, पेटी ले आओ ।
पेटी के रुपयों को गिनना प्रारम्भ कीजिए । दरवाजा बन्द है ?
देखो, बाहर कोई है तो नहीं ।
अब ग्राहकों का आना बन्द हो जाता है ।
दिन भर की आय का
लेखा-जोखा प्रारम्भ हो जाता है ।
दस-दस रुपये की,
सौ-सौ रुपये की अलग-अलग
गिड्डियाँ बनाकर तैयार की गईं ।
आय को देखकर खुश होता है
और कहता है कि
आज का दिन तो बहुत अच्छा हुआ ।
वाह, आज तो बहुत अधिक आय हो गई ।
उस खुशी में इतना अधिक लीन हो गया
कि कोई मित्र आ गया,
भाई आ गया, अन्य कोई भी आ गया
तो भी वह उनकी तरफ देख ही नहीं रहा है ।
वह आय में इतना मग्न है
कि बाहर कौन है ? क्या हो रहा है ?
कौन क्या कह रहा है ? कुछ भी भान नहीं है,
चूंकि आय के आनन्द में मग्न है ।
इस समय उसके पास कहीं से
फोन की घण्टी आती है
तो फोन भी नहीं उठाता
क्योंकि वह तो अपने प्रयोजन की
सफलता पर अत्यन्त प्रसन्न है ।
उसे अन्य किसी भी
प्रकार का विकल्प नहीं है ।
यह उसकी एक प्रकार से
निर्विकल्प दशा होती है ।
इससे पूर्व रुपयों की गिड्डी
गिनने आदि की क्रिया व्यवहार,
विकल्प की दशा थी ।
वह भी जरूरी होती है ।
यदि लेखा-जेखा नहीं रखता
तो आय का आनन्द कैसे आता ?
मुझसे हाई…को
कहा हो ? आओ…सिलक मिला लें
ओ ! मन मुनीम
आचार्य श्री जी
सोचो, विचार करो ।
इधर-उधर किसी के साथ की
प्रतीक्षा मत करो ।
कोई साथ हो तो देखेंगे ।
दुनिया में साथ देने वाला कोई भी नहीं है । अपना शरीर ही अपना साथ नहीं देता
तो अन्य किसी से क्या आशा करना ।
जहाँ देह अपनी नहीं,
तहाँ न अपना कोय
बारह भावना में प्रतिदिन
अन्यत्व भावना का चिन्तन करते ही हैं ।
अपना मन, वचन, काय ही
सहयोग नहीं देता
तो अन्य के सहयोग की अपेक्षा
कैसे की जा सकती है ।
फिर भी अपने मन को
समझाने पर समझ सकता है ।
यदि मन समझ गया
तो वचन और काय तो समझ ही जायेंगे,
लेकिन मन को समझाना बहुत कठिन है ।
मन ही ऐसा तत्व है
जो सारा संसार बनाकर
स्वयं खड़ा खड़ा देख रहा है
और मजा ले रहा है ।
विपरीत दिशा में कदम उठाता है
और कहता है
देखो, अब हम तो साथ नहीं देंगे,
मैंने बहुत साथ दिया है ।
फिर भी मन को बार-बार समझाना
आवश्यक होता है ।
समझाते समय मन नाराज हो
तो हो जाने दो ।
कब तक नाराज रहेगा ?
आखिर मन का स्त्रोत आत्मा से ही होता है ।
जैसे मुनीम जी दुकान पर बैठे हैं ।
यदि मुनीम अपने कार्य को छोड़कर
इधर-उधर की बात करने लगता है
तो मालिक कहता है
अब हमें मुनीम की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुनीम जी के कार्य का
निरीक्षण करने दूसरे मुनीम की
आवश्यकता पड़ रही है ।
इसमें व्यवस्था बिगड़ रही है ।
ऐसा कहने पर मुनीम के लिए
बात समझ में आ जाती है
और व्यवस्थित कार्य करने तैयार हो जाता है इसी प्रकार मन को नियन्त्रित करने के लिए
यदि मन को डाँटना पड़े
तो भी ठीक है,
मन नाराज हो जाये तो भी ठीक है,
क्योंकि बाद में
मुनीमजी के समान
जब बात समझ में आ जाती है,
तो मन भी स्वतः नियन्त्रित हो जाता है ।
साधक अपने मन को नियन्त्रित करके
इस प्रकार साधना के साँचे में ढ़ालता है
कि बाह्य पदार्थों से भी सम्बन्ध रखो
तो उनसे ही रखो,
जिनसे अन्तरंग सम्बन्ध में बाधा न हो ।
मुझसे हाई…को
लक्ष सहाई… जुड़ें
न बढ़ें…लक्ष्य ‘कि धरासाई
आचार्य श्री जी
आत्मा भी एक राजा है,
उसे जानो, श्रद्धान करो ।
जैसे ही आत्मा के स्वभाव के बारे में
जानने लग जाते हैं,
तत्त्व की ओर दृष्टिपात करने लग जाते हैं,
तो भव्य हो या अभव्य,
बन्ध की अपेक्षा
७० कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति को अन्तःकोडाकोडी सागर प्रमाण कर लेता है ।
यह सम्यग्दर्शन के पूर्व
होने वाली लब्धियों की विशेषता होती है । करणलब्धि के बिना
अभव्य को भी देशना, विशुद्धि,
क्षयोपशम और प्रायोग्य
ये चार लब्धियाँ हो जाती हैं ।
जिनके प्रभाव से वह कर्मबन्ध की
स्थितियों को अन्तःकोटाकोटि
सागर प्रमाण कर लेता है ।
यह कार्य मिथ्यात्व दशा में ही
अनन्तानुबन्धी कषाय के
उदय में ही हो जाता है ।
तत्त्व की ओर दृष्टि जाते ही,
शान्ति से बैठकर
चिन्तन करने में उपयोग की एकाग्रता होने से बहुत बड़े-बड़े कार्य सफल हो जाते हैं ।
मोक्षमार्ग में हाथ-पैर चलाने की
या फावड़ा चलाने के श्रम की
आवश्यकता नहीं होती ।
यहाँ मानसिक, शारीरिक या वाचनिक
परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं होती ।
बस, बाहर से भीतर की ओर अपने स्वभाव में आने की आवश्यकता होती है ।
मैं कौन हूँ ?
इसके बारे में जब तक विचार नहीं आता
तब तक कुछ नहीं हो सकता ।
कहते हैं-
दुष्टन देहु निकार, साधुन को रख लीजै ।
कर्म को दुष्ट कहते हैं
जबकि वह तो जड़ है ।
यह कर्म आखिर क्यों बंधता है ?
इसका कारण ढूँढ़ो ?
आचार्य कहते हैं
अज्ञानी प्राणी अज्ञान दशा में
कर्मबन्ध कर लेते हैं ।
उनके उदय होने पर
कोई बचाने वाला नहीं होता ।
मैं कौन हूँ ? इस प्रश्न के अभाव में
हमारा अनन्त अतीत कैसे चला गया ।
इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं,
कुछ विचार ही नहीं किया,
अभी भी नहीं सोचते ।
‘तत्त्वचिन्तन में हमारे कितने क्षणों का
सदुपयोग होता है,
इसका लेखा-जोखा रखना चाहिए।’
आज तक हमारा उपयोग बहिर्मुखी बना रहा बाह्य पर पदार्थों को ही
अपना विषय बनाता रहा ।
वर्षा होती है,
उस समय सीप के मुख में
जल की एकाध बूँद गिरती है
और स्वाति नक्षत्र का योग होता है
तो वही जल मोती बन जाती है ।
मात्र अन्तर्मुहूर्त का काम है,
परन्तु अनन्तकाल व्यतीत हो गया
तो भी नहीं कर पाये ।
जानना देखना ही आत्मा का स्वभाव है,
इसका श्रद्धान करो,
इसे सम्यक् रूपेण जानने का प्रयास करो ।
मुझसे हाई…को
सोचूँ जरा,
मैं कौन हूँ…
आया कहाँ से, जाना कहाँ ?
आचार्य श्री जी
विद्यार्थी जब पेपर देता है
उस समय वह यह नहीं सोचता है
कि कौन-सी कक्षा का छात्र हूँ ।
परीक्षा तो परीक्षा होती है,
चाहे किसी भी कक्षा की हो ।
वह पूरे वर्ष पढ़ाई करता है,
पढ़ाई तो ३६५ दिन करता है
परन्तु पेपर देने के तो
मात्र तीन घण्टे ही होते हैं ।
जो प्रतिभा सम्पन्न छात्र होता है
वह शीघ्रता से पेपर हल करता जाता है ।
तीन घण्टे का समय पता ही नहीं चलता,
बल्कि उसे समय कम पड़ जाता है
और आप लोगों से
उत्कृष्ट सामायिक का कहा जाये
तो मन नहीं लगता,
पैरों में दर्द होने लगता है,
मन एकाग्र नहीं होता ।
जबकि सामायिक आपके लिए श्रेयस्कर है । विचार करो,
गिरि- गुफाओं में कैसे दिन कटते होंगे ?
गुफाओं में ध्यान करने वाले
मुनिराजों का सुख कैसा होता है ?
छहढाला में कहा है
सो इन्द्र नाग नरेन्द्र व,
अहमिन्द्र को नाहीं कह्यो ।
जैसा सुख उन साधक श्रमणों को होता है
वैसा इन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र,
और अहमिन्द्रों को भी नहीं होता ।
जिस प्रकार व्रती अपने व्रतों की सीमा में
बंध जाता है
उसे कोई करोड़ों रुपये का भी प्रलोभन दें
तो भी वह अपनी सीमा का
उल्लंघन नहीं करता ।
उसी प्रकार निर्विकल्पसमाधि वाला
साधक भी अपने आप में आत्मसंतोष
एवं आत्मतृप्ति को प्राप्त होता है
कि बाहर का कोई भी प्रलोभन
उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता । जो साधक बाह्य वस्तु के प्रलोभन में
आ जाता है,
कोई भी मानसिक परीषह
या शब्दों की चपेट में आ जाता है
वह कभी निर्विकल्प नहीं हो सकता ।् निर्विकल्प समाधि में रहना,
यह साधक की परीक्षा का समय माना जाता है । विद्यार्थी की भाँति ३६५ दिन साधना करता है और बीच में जब-जब निर्विकल्पसमाधि का समय आता है
उस समय उसका पेपर होता है ।
जो साधना में दृढ़ होता है
वह प्रतिभासम्पन्न छात्र की भाँति
अपना पेपर शीघ्रता से,
एकाग्रता से हल कर देता है ।
यहाँ-वहाँ अपना उपयोग चंचल नहीं करते । प्रशंसा या निन्दा के वचन सुनकर भी
वे उनसे प्रभावित नहीं होते ।
बल्कि वे सोचते हैं
कि हमारा स्वभाव तो ज्ञानस्वरूप है,
इसे ये जानते ही नहीं हैं,
इसलिए ये हमारी क्या प्रशंसा करेंगे ?
और यदि मेरे स्वरूप को जानते हैं
तो ये मेरी क्या निन्दा करेंगे ?
क्योंकि मेरा ज्ञान स्वभाव
निन्दा का विषय ही नहीं है ।
इस प्रकार चिन्तन के द्वारा
प्रशंसा और निन्दा के विकल्पों को तोड़ देता है । आत्मचिन्तन या आत्मानुभव में
इन विकल्पों को स्थान ही नहीं रहता ।
मुझसे हाई…को
सुख वैसा न अहमिन्द को,
जैसा अहम्-मन्द को
आचार्य श्री जी
असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव
अतीत अनागत के बारे में
कुछ सोच सकता ।
ये सभी विकल्प संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव के
ही होते हैं ।
यह अतीत-अनागत सम्बन्धी
मन की उपज है ।
बिना मन के मात्र इन्द्रियाँ
अतीत को अपना विषय नहीं बना सकतीं ।
अतः इन्द्रियाँ नहीं
किन्तु मन खतरनाक होता है ।
भले ही इसके पास नाक नहीं है,
फिर भी खतरनाक है, टेढ़ा है ।
मैं वह था, मैं वह हूँ, वह रहूँगा, इत्यादि
विकल्प मन के द्वारा ही होते हैं ।
जिसका मन जितना जितना
निर्विकल्प होता जाता है
उतना-उतना कल्याण के मार्ग पर
आगे बढ़ सकता है ।
बालक के समान कम कषाय वाला मन ही
जल्दी कल्याण कर सकता है
जैसे बालक को माँ ने चाँटा मारा
तो वह रोने लगता है ।
उसी समय रोते हुए को
यदि माँ ने किसी भी तरह से मना लिया
तो वह शान्त हो जाता है ।
किसी ने खुश कि खुश हो जाता है ।
माँ के मारे हुए चाँटे को शीघ्र ही भूल जाता है । यदि वह चाटे को याद रखता
तो खुश नहीं हो सकता है ।
बच्चे जब बड़े हो जाते हैं
तो वे छोटे बच्चों की भाँति
सहज और सरल नहीं रह पाते ।
उनमें टेढ़ापन का प्रवेश हो जाता है ।
वे किसी भी बात को शीघ्र ही
सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं ।
इसी प्रकार जिस साधक का मन
छोटे बालक की भाँति
या तुरन्त उत्पन्न बालक की भाँति
सरल और सहज होता है,
टेढ़ापन नहीं रहता,
कषाय का तीव्र आवेग नहीं रहता
वही साधक कल्याण के मार्ग पर
स्वयं भी आगे बढ़ता है
और अन्य साधकों को भी
कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाने में
सफल होता है ।
यदि साधक का अपनी कषाय के
वेग पर नियन्त्रण नहीं होता
तो वह कल्याण के मार्ग पर
स्वयं अग्रसर नहीं हो सकता है ।
जो स्वयं कल्याण पथ पर
आगे नहीं बढ़ सकता
वह दूसरों को कल्याण के मार्ग पर
आगे बढ़ने में कारण कैसे बन सकता है ?
अतः बालक के समान कम कषाय ही
जल्दी से कल्याण कर सकता है ।
मुझसे हाई…को
बचा कषाय से
बच्चा बनो किसी भी उपाय से
Sharing is caring!
© Copyright 2021 . Design & Deployment by : Coder Point
© Copyright 2021 . Design & Deployment by : Coder Point